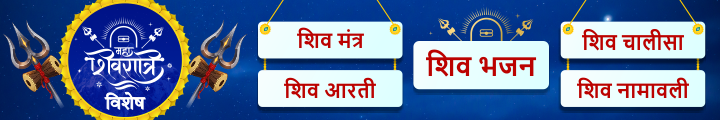गूगल पर भक्ति भारत को अपना प्रीफ़र्ड सोर्स बनाएँ


शिव ने शिवा को बताया भक्ति क्या है? (Shiv told Shiva What is Bhakti?)
भगवान शिव ने देवी शिवा अर्थात आदिशक्ति महेश्वरी सती को उत्तम भक्तिभाव के बारे मे इस प्रकार बताया.. अरुणोदयमारभ्य सेवाकालेऽञ्चिता हृदा।
निर्भयत्वं सदा लोके स्मरणं तदुदाहृतम्॥२८
अरुणोदयकालसे प्रारम्भकर शयनपर्यन्त तत्पर चित्तसे निर्भय होकर भगवद्विग्रहकी सेवा करनेको स्मरण कहा जाता है [ यह सगुण स्मरण भक्ति है।] २८
सदा सेव्यानुकूल्येन सेवनं तद्धि गोगणैः।
हृदयामृतभोगेन प्रियं दास्यमुदाहृतम्॥२९
हर समय सेव्यकी अनुकूलताका ध्यान रखते हुए हृदय और इन्द्रियोंसे जो निरन्तर सेवा की जाती है, वही सेवन नामक भक्ति है। अपनेको प्रभुका किंकर समझकर हृदयामृतके भोगसे स्वामीका सद्ा प्रिय-सम्पादन करना दास्य कहा गया है॥ २९
सदा भृत्यानुकूल्येन विधिना मे परात्मने।
अर्पणं षोडशानां वै पाद्यादीनां तदर्चनम्॥ ३०
अपनेको सदा सेवक समझकर शास्त्रीय विधिसे मुझ परमात्माको सदा पाद्य आदि सोलह उपचारोंका जो समर्पण करना है, उसे अर्चन कहा जाता है॥३०
मंत्रोच्चारणध्यानाभ्यां मनसा वचसा क्रमात्।
यदष्टाङ्गेन भूस्पर्शं तद्वै वंदनमुच्यते॥३१
वाणीसे मन्त्रका उच्चारण करते हुए तथा मनसे ध्यान करते हुए आठों अंगोंसे भूमिका स्पर्श करते हुए जो इष्टदेवको अष्टांग प्रणाम* किया जाता है, उसे वन्दन कहा जाता है॥ ३१
मङ्गलामङ्गलं यद्यत्करोतीतीश्वरो हि मे।
सर्वं तन्मङ्गलायेति विश्वास: सख्यलक्षणम्॥३२
ईश्वर मंगल-अमंगल जो कुछ भी करता है, वह सब मेरे मंगलके लिये है-ऐसा दृढ़ विश्वास रखना सख्य भक्तिका लक्षण है॥ ३२॥
कृत्वा देहादिकं तस्य प्रीत्यै सर्वं तदर्पणम्।
निर्वाहाय च शून्यत्वं यत्तदात्मसमर्पणम्॥३३
देह आदि जो कुछ भी अपनी कही जानेवाली वस्तु है, वह सब भगवान्की प्रसन्नताके लिये उन्हींको समर्पित करके अपने निर्वाहके लिये कुछ भी बचाकर न रखना अथवा निर्वाहकी चिन्तासे भी रहित हो जाना, आत्मसमर्पण कहा जाता है॥३३
नवाङ्गानीति मद्धक्तेर्भुक्तिमुक्तिप्रदानि च।
मम प्रियाणि चातीव ज्ञानोत्पत्तिकराणि च। ३४
उपाङ्गानि च मद्धक्तेर्बहूनि कथितानि वै।
बिल्वादिसेवनादीनि समूह्यानि विचारतः॥ ३५
मेरी भक्तिके ये नौ अंग हैं, जो भोग तथा मोक्ष प्रदान करनेवाले हैं। इनसे ज्ञान प्रकट हो जाता है तथा ये साधन मुझे अत्यन्त प्रिय हैं। मेरी भक्तिके अनेक उपांग भी कहे गये हैं। जैसे बिल्व आदिका सेवन, इनको विचारसे समझ लेना चाहिये॥ ३४-३५॥
इत्थं साङ्गोपाङ्गभक्तिर्मम सर्वोत्तमा प्रिये।
ज्ञानवैराग्यजननी मुक्तिदासी विराजते॥ ३६
सर्वकर्मफलोत्पत्तिः सर्वदा त्वत्समप्रिया।
यच्चित्ते सा स्थिता नित्यं सर्वदा सोऽति मत्प्रियः ॥ ३७
हे प्रिये! इस प्रकार मेरी सांगोपांग भक्ति सबसे उत्तम है। यह ज्ञान-वैराग्यकी जननी है और मुक्ति इसकी दासी है। हे देवि! भक्ति सर्वदा सभी कर्मोंक फलोंको देनेवाली है, यह भक्ति मुझे सदा तुम्हारे समान ही प्रिय है। जिसके चित्तमें नित्य-निरन्तर यह भक्ति निवास करती है, वह मुझे अत्यन्त प्रिय है॥ ३६-३७
ब्रैलोक्ये भक्तिसदृशः पंथा नास्ति सुखावहः।
वतु्युगेषु देवेशि कलौ तु सुविशेषतः ॥३८
कलौ तु ज्ञानवैराग्यौ वृद्धरूपौ निरुत्सवौ।
ग्राहकाभावतो देवि जातौ जर्जरतामति॥३९
हे देवेशि! तीनों लोकों और चारों युगोंमें भक्तिके समान दूसरा कोई सुखदायक मार्ग नहीं है। कलियुगमें तो यह विशेष सुखद एवं सुविधाजनक है; क्योंकि कलियुगमें प्रायः ज्ञान और वैराग्य दोनों ही ग्राहकके अभावके कारण वृद्ध, उत्साहशून्य और जर्जर हो जाते हैं॥ ३८-३९॥
कलौ प्रत्यक्षफलदा भक्तिः सर्वयुगेष्वपि।
तत्प्रभावादहं नित्यं तद्वशो नात्र संशयः॥४०
परंतु भक्ति कलियुगमें तथा अन्य सभी युगोंमें भी प्रत्यक्ष फल देनेवाली है। भक्तिके प्रभावसे मैं सदा भक्तके वशमें रहता हूँ, इसमें सन्देह नहीं है॥४०
यो भक्तिमान्पुमॉँल्लोके सदाहं तत्सहायकृत्।
विघ्नहर्ता रिपुस्तस्य दंड्यो नात्र च संशयः॥४१
संसारमें जो भक्तिमान् पुरुष है, उसकी मैं सदा सहायता करता हूँ और उसके कष्टोंको दूर करता हूँ। उस भक्तका जो शत्रु होता है, वह मेरे लिये दण्डनीय है, इसमें संशय नहीं है॥४१
भक्तहेतोरहं देवि कालं क्रोधपरिप्लुतः।
अदहं वह्निना नेत्रभवेन निजरक्षकः॥४२
हे देवि! मैं अपने भक्तोंका रक्षक हूँ, भक्तकी रक्षाके लिये ही मैंने कुपित होकर अपने नेत्रजनित अग्निसे कालको भी भस्म कर डाला था॥ ४२
भक्तहेतोरहं देवि रव्युपर्यभवं किल।
अतिक्रोधान्वितः शूलं गृहीत्वान्वजयं पुरा॥४३
हे देवि! भक्तकी रक्षाके लिये मैं पूर्वकालमें सूर्यपर भी अत्यन्त क्रोधित हो उठा था और मैंने त्रिशूल लेकर सूर्यको भी जीत लिया था॥४३॥
भक्तहेतोरहं देवि रावणं सगणं क्रुधा।
त्यजामि स्म कृतो नैव पक्षपातो हि तस्य वै॥४४
भक्तहेतोरहं देवि व्यासं हि कुमतिग्रहम्।
काश्या न्यसारयं क्रोधाद्दण्डयित्वा च नंदिना॥ ४५
हे देवि! मैंने भक्तके लिये सैन्यसहित रावणको भी क्रोधपूर्वक त्याग दिया और उसके प्रति कोई पक्षपात नहीं किया। हे देवि! भक्तोंके लिये ही मैंने कुमतिसे ग्रस्त व्यासको नन्दीद्वारा दण्ड दिलाकर उन्हें काशीके बाहर निकाल दिया॥४४-४५
किं बहूक्तेन देवेशि भक्ताधीनः सदा ह्यहम्।
तत्कर्तु: पुरुषस्यातिवशगो नात्र संशयः॥४६
हे देवेशि! बहुत कहनेसे क्या लाभ, मैं सदा ही भक्तके अधीन रहता हूँ और भक्ति करनेवाले पुरुषके अत्यन्त वशमें हो जाता हूँ, इसमें सन्देह नहीं है॥४६
[श्रीशिवमहापुराण / रुद्रसंहिता / सतीखण्ड / 23 ]
निर्भयत्वं सदा लोके स्मरणं तदुदाहृतम्॥२८
अरुणोदयकालसे प्रारम्भकर शयनपर्यन्त तत्पर चित्तसे निर्भय होकर भगवद्विग्रहकी सेवा करनेको स्मरण कहा जाता है [ यह सगुण स्मरण भक्ति है।] २८
सदा सेव्यानुकूल्येन सेवनं तद्धि गोगणैः।
हृदयामृतभोगेन प्रियं दास्यमुदाहृतम्॥२९
हर समय सेव्यकी अनुकूलताका ध्यान रखते हुए हृदय और इन्द्रियोंसे जो निरन्तर सेवा की जाती है, वही सेवन नामक भक्ति है। अपनेको प्रभुका किंकर समझकर हृदयामृतके भोगसे स्वामीका सद्ा प्रिय-सम्पादन करना दास्य कहा गया है॥ २९
सदा भृत्यानुकूल्येन विधिना मे परात्मने।
अर्पणं षोडशानां वै पाद्यादीनां तदर्चनम्॥ ३०
अपनेको सदा सेवक समझकर शास्त्रीय विधिसे मुझ परमात्माको सदा पाद्य आदि सोलह उपचारोंका जो समर्पण करना है, उसे अर्चन कहा जाता है॥३०
मंत्रोच्चारणध्यानाभ्यां मनसा वचसा क्रमात्।
यदष्टाङ्गेन भूस्पर्शं तद्वै वंदनमुच्यते॥३१
वाणीसे मन्त्रका उच्चारण करते हुए तथा मनसे ध्यान करते हुए आठों अंगोंसे भूमिका स्पर्श करते हुए जो इष्टदेवको अष्टांग प्रणाम* किया जाता है, उसे वन्दन कहा जाता है॥ ३१
मङ्गलामङ्गलं यद्यत्करोतीतीश्वरो हि मे।
सर्वं तन्मङ्गलायेति विश्वास: सख्यलक्षणम्॥३२
ईश्वर मंगल-अमंगल जो कुछ भी करता है, वह सब मेरे मंगलके लिये है-ऐसा दृढ़ विश्वास रखना सख्य भक्तिका लक्षण है॥ ३२॥
कृत्वा देहादिकं तस्य प्रीत्यै सर्वं तदर्पणम्।
निर्वाहाय च शून्यत्वं यत्तदात्मसमर्पणम्॥३३
देह आदि जो कुछ भी अपनी कही जानेवाली वस्तु है, वह सब भगवान्की प्रसन्नताके लिये उन्हींको समर्पित करके अपने निर्वाहके लिये कुछ भी बचाकर न रखना अथवा निर्वाहकी चिन्तासे भी रहित हो जाना, आत्मसमर्पण कहा जाता है॥३३
नवाङ्गानीति मद्धक्तेर्भुक्तिमुक्तिप्रदानि च।
मम प्रियाणि चातीव ज्ञानोत्पत्तिकराणि च। ३४
उपाङ्गानि च मद्धक्तेर्बहूनि कथितानि वै।
बिल्वादिसेवनादीनि समूह्यानि विचारतः॥ ३५
मेरी भक्तिके ये नौ अंग हैं, जो भोग तथा मोक्ष प्रदान करनेवाले हैं। इनसे ज्ञान प्रकट हो जाता है तथा ये साधन मुझे अत्यन्त प्रिय हैं। मेरी भक्तिके अनेक उपांग भी कहे गये हैं। जैसे बिल्व आदिका सेवन, इनको विचारसे समझ लेना चाहिये॥ ३४-३५॥
इत्थं साङ्गोपाङ्गभक्तिर्मम सर्वोत्तमा प्रिये।
ज्ञानवैराग्यजननी मुक्तिदासी विराजते॥ ३६
सर्वकर्मफलोत्पत्तिः सर्वदा त्वत्समप्रिया।
यच्चित्ते सा स्थिता नित्यं सर्वदा सोऽति मत्प्रियः ॥ ३७
हे प्रिये! इस प्रकार मेरी सांगोपांग भक्ति सबसे उत्तम है। यह ज्ञान-वैराग्यकी जननी है और मुक्ति इसकी दासी है। हे देवि! भक्ति सर्वदा सभी कर्मोंक फलोंको देनेवाली है, यह भक्ति मुझे सदा तुम्हारे समान ही प्रिय है। जिसके चित्तमें नित्य-निरन्तर यह भक्ति निवास करती है, वह मुझे अत्यन्त प्रिय है॥ ३६-३७
ब्रैलोक्ये भक्तिसदृशः पंथा नास्ति सुखावहः।
वतु्युगेषु देवेशि कलौ तु सुविशेषतः ॥३८
कलौ तु ज्ञानवैराग्यौ वृद्धरूपौ निरुत्सवौ।
ग्राहकाभावतो देवि जातौ जर्जरतामति॥३९
हे देवेशि! तीनों लोकों और चारों युगोंमें भक्तिके समान दूसरा कोई सुखदायक मार्ग नहीं है। कलियुगमें तो यह विशेष सुखद एवं सुविधाजनक है; क्योंकि कलियुगमें प्रायः ज्ञान और वैराग्य दोनों ही ग्राहकके अभावके कारण वृद्ध, उत्साहशून्य और जर्जर हो जाते हैं॥ ३८-३९॥
कलौ प्रत्यक्षफलदा भक्तिः सर्वयुगेष्वपि।
तत्प्रभावादहं नित्यं तद्वशो नात्र संशयः॥४०
परंतु भक्ति कलियुगमें तथा अन्य सभी युगोंमें भी प्रत्यक्ष फल देनेवाली है। भक्तिके प्रभावसे मैं सदा भक्तके वशमें रहता हूँ, इसमें सन्देह नहीं है॥४०
यो भक्तिमान्पुमॉँल्लोके सदाहं तत्सहायकृत्।
विघ्नहर्ता रिपुस्तस्य दंड्यो नात्र च संशयः॥४१
संसारमें जो भक्तिमान् पुरुष है, उसकी मैं सदा सहायता करता हूँ और उसके कष्टोंको दूर करता हूँ। उस भक्तका जो शत्रु होता है, वह मेरे लिये दण्डनीय है, इसमें संशय नहीं है॥४१
भक्तहेतोरहं देवि कालं क्रोधपरिप्लुतः।
अदहं वह्निना नेत्रभवेन निजरक्षकः॥४२
हे देवि! मैं अपने भक्तोंका रक्षक हूँ, भक्तकी रक्षाके लिये ही मैंने कुपित होकर अपने नेत्रजनित अग्निसे कालको भी भस्म कर डाला था॥ ४२
भक्तहेतोरहं देवि रव्युपर्यभवं किल।
अतिक्रोधान्वितः शूलं गृहीत्वान्वजयं पुरा॥४३
हे देवि! भक्तकी रक्षाके लिये मैं पूर्वकालमें सूर्यपर भी अत्यन्त क्रोधित हो उठा था और मैंने त्रिशूल लेकर सूर्यको भी जीत लिया था॥४३॥
भक्तहेतोरहं देवि रावणं सगणं क्रुधा।
त्यजामि स्म कृतो नैव पक्षपातो हि तस्य वै॥४४
भक्तहेतोरहं देवि व्यासं हि कुमतिग्रहम्।
काश्या न्यसारयं क्रोधाद्दण्डयित्वा च नंदिना॥ ४५
हे देवि! मैंने भक्तके लिये सैन्यसहित रावणको भी क्रोधपूर्वक त्याग दिया और उसके प्रति कोई पक्षपात नहीं किया। हे देवि! भक्तोंके लिये ही मैंने कुमतिसे ग्रस्त व्यासको नन्दीद्वारा दण्ड दिलाकर उन्हें काशीके बाहर निकाल दिया॥४४-४५
किं बहूक्तेन देवेशि भक्ताधीनः सदा ह्यहम्।
तत्कर्तु: पुरुषस्यातिवशगो नात्र संशयः॥४६
हे देवेशि! बहुत कहनेसे क्या लाभ, मैं सदा ही भक्तके अधीन रहता हूँ और भक्ति करनेवाले पुरुषके अत्यन्त वशमें हो जाता हूँ, इसमें सन्देह नहीं है॥४६
[श्रीशिवमहापुराण / रुद्रसंहिता / सतीखण्ड / 23 ]
यह भी जानें
- राम जपते रहो काम करते रहो
- भगवान बुद्ध वंदना
- श्री राम स्तुति
- राम मंदिर सोमनाथ
- राम नवमी
- कुंज बिहारी श्री गिरधर कृष्ण मुरारी
- श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी
- कृष्णा चालीसा
- श्री दशावतार स्तोत्र: प्रलय पयोधि-जले
- ॐ जय जगदीश हरे आरती
Blogs Bhakti BlogsDevi Shiva BlogsMonday BlogsSomwar BlogsShivling BlogsMata Sati BlogsShiv Mahapuran BlogsRudra Samhita BlogsSati Khand Blogs
अगर आपको यह ब्लॉग पसंद है, तो कृपया शेयर, लाइक या कॉमेंट जरूर करें!
 भक्ति-भारत वॉट्स्ऐप चैनल फॉलो करें »
भक्ति-भारत वॉट्स्ऐप चैनल फॉलो करें »
इस ब्लॉग को भविष्य के लिए सुरक्षित / बुकमार्क करें
* कृपया अपने किसी भी तरह के सुझावों अथवा विचारों को हमारे साथ अवश्य शेयर करें।
 भक्ति-भारत वॉट्स्ऐप चैनल फॉलो करें »
भक्ति-भारत वॉट्स्ऐप चैनल फॉलो करें »इस ब्लॉग को भविष्य के लिए सुरक्षित / बुकमार्क करें
* कृपया अपने किसी भी तरह के सुझावों अथवा विचारों को हमारे साथ अवश्य शेयर करें।
** आप अपना हर तरह का फीडबैक हमें जरूर साझा करें, तब चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक: यहाँ साझा करें।
भक्ति-भारत विशेष:
- दिल्ली मे माता के प्रसिद्ध मंदिर
- दिल्ली के कालीबाड़ी मंदिर
- भारत के चार धाम
- द्वादश ज्योतिर्लिंग
- सप्त मोक्ष पुरी
- ब्रजभूमि के प्रसिद्ध मंदिर
- प्रसिद्ध इस्ककों टेंपल्स
- बिरला के प्रसिद्ध मंदिर
- महाभारत काल से दिल्ली के प्रसिद्ध मंदिर
- दिल्ली के प्रसिद्ध शिव मंदिर
- दिल्ली के प्रसिद्ध हनुमान बालाजी मंदिर
- दिल्ली और आस-पास के प्रसिद्ध मंदिर
- सिरसागंज के प्रसिद्ध मंदिर